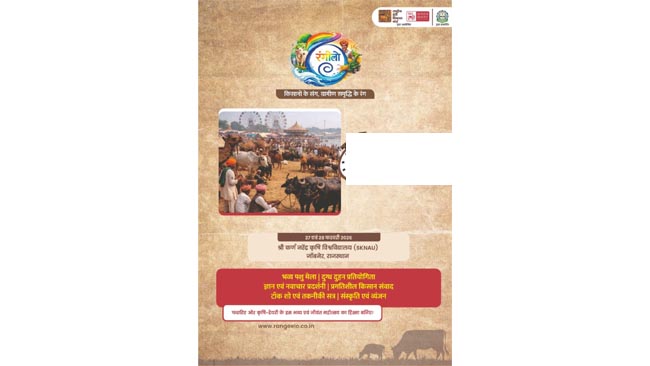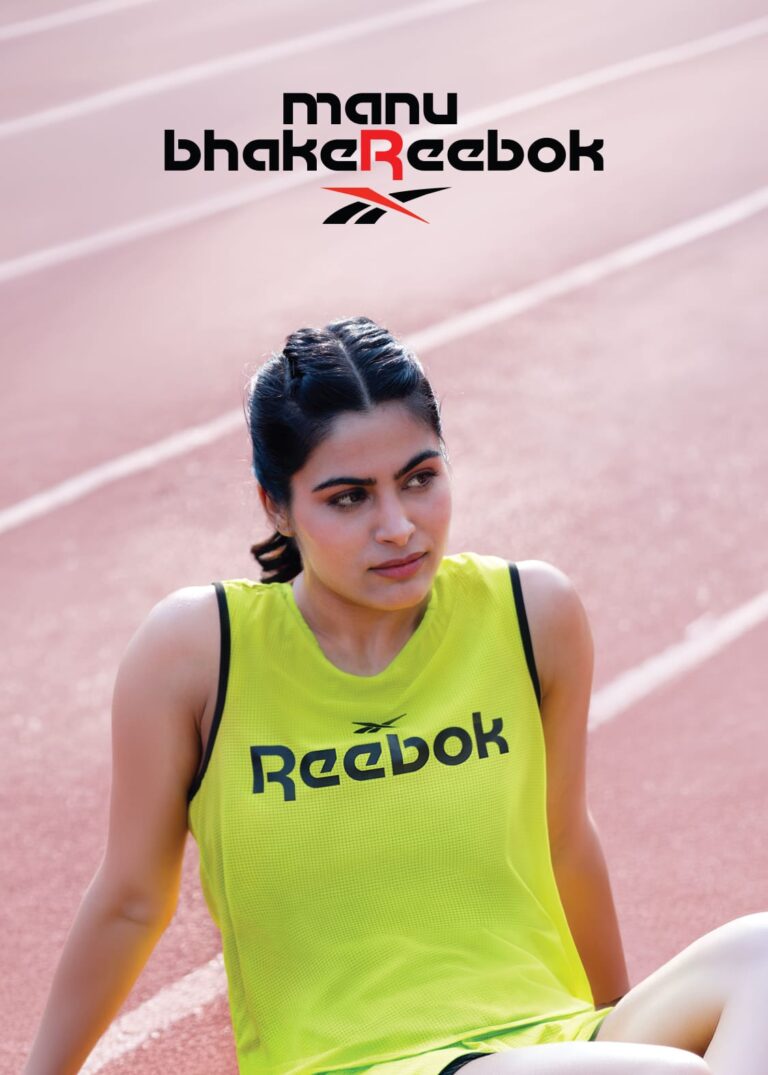संघ के शताब्दी वर्ष पर पांच प्रबोधन कार्यों में से एक है सामाजिक समरसता

जयपुर। सामाजिक समरसता का एक अर्थ-व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास करना है। जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार की क्षमता लेकर पैदा होता है। उसकी क्षमता के विकास का उसे अवसर देना, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहनराव भागवत ने संघ के शताब्दी वर्ष पर पांच प्रबोधन कार्यों में से एक सामाजिक समरसता को भी स्थान दिया है। संघ का मानना है कि समाज में हो रहे भेदभाव को मिटाकर सभी जाति वर्ग के लोग समरस हो जाए । इसका तात्पर्य जिस प्रकार शर्बत में चीनी घुल जाती है, उसी प्रकार सभी समाज के लोग आपस में घुल-मिल जाए।
अमेरिका के प्रख्यात विचारक एवं तृतीय राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था कि ‘हम सभी के मन और हृदय को एक होने दें।’ सामाजिक सम्मेलन को बढ़ाएं , इसके बिना स्वतंत्रता और जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। इन शब्दों में जेफरसन अमेरिका की जनता से कहते है कि ‘सामाजिक समरसता का निर्माण करें, तभी आपकी स्वतंत्रता कायम रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर (श्री गुरूजी) ने हिन्दू समाज की इस कुरीति को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए। उनका पूरा नाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर था, उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एमएससी करने के बाद अध्यापन कार्य भी कराया, जिसमें वे ‘गुरूजी” के नाम से विख्यात हुए। गुरुजी ने कहा कि अस्पृश्यता हिन्दू समाज की सबसे हानिकारक व्याधि है। इसने सामाजिक प्रगति, संतुलन और सद्भाव को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। यह एक विकार या दोष मात्र न होकर सभ्य समाज के लिए काजल से भी अधिक काला कलंक है, जो हिन्दू समाज के मूल चरित्र को नष्ट करता है। भ्रातृत्व, उदार मन और समानता का भाव प्रत्येक हिन्दू की मौलिक प्रकृति और लक्ष्य दोनों होता है। अस्पृष्यता के प्रवेश ने स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण को ही नष्ट करने का काम किया है। इसे ठीक करने के लिए बहुआयामी प्रयासों की जरूरत है। अस्पृश्यता हिन्दू समाज पर लगा सबसे बड़ा कलंक है।
श्री गुरूजी ने कोट करते हुए लिखा-‘राजस्थान के एक गांव में एक हरिजन युवक को इस कारण पीट-पीटकर मार डाला गया, क्योंकि उसने मूंछें बढ़ा रखी थीं, जो केवल क्षत्रियों का ही‘ विषेषाधिकार‘ माना जाता था। हमारे धर्माचार्य भी ऐसे आचरण की निंदा नहीं करते, क्योंकि गलती से वे कुप्रथाओं को ‘धर्म‘ मान बैठे हैं। इस घटना से समझा जा सकता है कि श्रीगुरुजी सामाजिक अस्पृश्यता को दूर करना चाहते थे। वे अस्पृश्यता को हिन्दू समाज पर एक बड़ा कलंक मानते थे।
गुरुजी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए 29 अगस्त,1964 को मुंबई में स्वामी चिन्मयानंद जी के संदीपनी आश्रम में अनेक संप्रदायों के प्रमुखों की उपस्थिति में ‘विश्व हिन्दू परिषद” की स्थापना की थी। इस अवसर पर गुरुजी ने समाज के पिछड़े और निर्धन वर्गों के प्रति समाज एवं उसके धर्म गुरुओं के दायित्व का उल्लेख किया। 11, 12 और 13 जनवरी, 1966 को प्रयाग के कुंभ मेले के अवसर पर विहिप के प्रथम अधिवेशन में गुरुजी के अनुरोध पर संतों ने ‘ हिन्दुः न पतितो भवेत’ (हिन्दू पतित नहीं होता) जैसी घोषणा करके अशिक्षा और गरीबी के कारण धर्मान्तरितों को समाज में वापस लौटने का मार्ग खोल दिया था। इसके लिए शंकराचार्यो एवं संत व्यक्ति की मानसिक सिद्धता तैयार करवा दी। एक बार गुरुजी से पूछा गया कि ‘अस्पृश्यता की समस्या कैसे हल होगी?’ इस पर गुरुजी ने कहा कि यह समस्या जितनी जल्दी हो सुलझ जाए। ‘अस्पृश्यता निवारण अभियान’ का ढिढोरा पीटते हुए कदम उठाने से ‘ निवारण’ के बजाय संघर्ष ही बढ़ता है और दुराग्रह निर्माण होकर एक नई समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि अस्पृश्य माने जाने वालों को शुद्धीकरण करने से भी अत्यन्त सरल कोई विधि तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि अपने घर में यदि कोई बीमार हो जाए तो स्वयं कष्ट उठाकर भी हम सब कुछ करते ही हैं, वह कार्य यहां भी लागू है। अपने ही घर का व्यक्ति बीमार है, ऐसा मानकर त्याग भाव से अन्य सभी लोगों को भरसक प्रयत्न करना होगा। सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर सम्पूर्ण हिन्दू जगत का आह्वान किया गया कि वे श्रद्धेय आचार्यों व धर्मगुरूओं के निर्देशानुसार
अपने समस्त धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठानों से अस्पृश्यता को निकाल बहार करें। उनका कहना था कि सामाजिक और धार्मिक क्रिया-कलापों में ऊंच-नीच या स्पृश्य-अस्पृश्य का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी हिन्दुओं को एक परिवार के रूप में रहना चाहिए। इस घोषणा पत्र को सभी धर्माचार्यों ने स्वीकार कर लिया। इस सम्मेलन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, धार्मिक प्रमुख और संन्यासी उपस्थित थे, इसमें सर्वमत, सर्व समर्थन और अत्यंत उत्साह के वातावरण में उक्त घोषणा-पत्र को स्वीकार किया गया। गुरुजी, पेजावर स्वामीजी और अन्य वक्ताओं ने इस प्रस्ताव को व्यवहार में लाने की मार्मिक अपील की थी। इसे एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा कि यह प्रस्ताव उसी उडुपी में पारित किया गया, जहां श्री कृष्ण के विग्रह ने जातिगत भेदभाव बरतने वालों की ओर अपनी पीठ कर दी थी। इन सब बातों से यही स्पष्ट होता है कि अस्पृश्यता कोई धार्मिक प्रथा नहीं है। यह एक दूषित सामाजिक प्रथा है, जिसका शास्त्र -सम्मत कोई धार्मिक आधार नहीं है। गुरूजी ने कहा कि अस्पृश्यता रोग की जड़ जनसामान्य के इस विश्वास में निहित है कि यह धर्म का अंग है और इसका उल्लंघन महापाप होगा। यह विकृत धारणा ही वह मूल कारण है, जिससे शताब्दी से अनेक समाज-सुधारकों एवं धर्म-धुरंधरों के समर्पित प्रयासों के बाद भी यह घातक परम्परा जनसामान्य के मन में आज भी घर किए बैठी है। अनेक महापुरूषों ने हिन्दू समाज के मस्तक पर लगे इस कलंक को मिटाने का अथक प्रयास किया। फिर भी यह कलुषित दाग अभी विधमान है। आज भी तथाकथित उच्च जातीय लोग उन तथाकथित अस्पृश्यता को अपने समान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक ही समाज की संतान हैं और हमें अपने सुख दुख परस्पर बांटने हैं। इस एकात्मभाव का अभाव ही हमारी दुर्गति का मूल कारण है। समाज के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण ठोस रूप में प्रकट होना चाहिए। जैसे हमारे समाज में अनेक लोगों को दैनिक भोजन के बिना रहना पड़ता है, क्या हम उनके प्रति संवेदनशील हैं? क्या हमारे मन में उनके लिए कुछ करने की इच्छा जागृत होती है? प्राचीनकाल में हमारे यहां‘ बलि वैष्वदेव यज्ञ’ होता था, जहां सर्व प्रथम निर्धन व भूखों को भोजन कराया जाता था, बाद में सब खाते थे। गुरुजी ने लिखा है कि तथाकथित अस्पृश्य जातियां मन-मस्तिष्क संबंधी गुणों में आनुवंशिक रूप से ही अक्षम हैं और वे आने वाले दीर्धकाल तक शेष समाज के स्तर तक नहीं पहुंच सकती, इनका अपमान ही नहीं, बल्कि तथ्यों का विडंबनापूर्ण उपहास भी है। इतिहास साक्षी है कि गत एक हजार वर्षों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में ये तथाकथित अस्पृश्य ही अग्रणी रहे हैं।