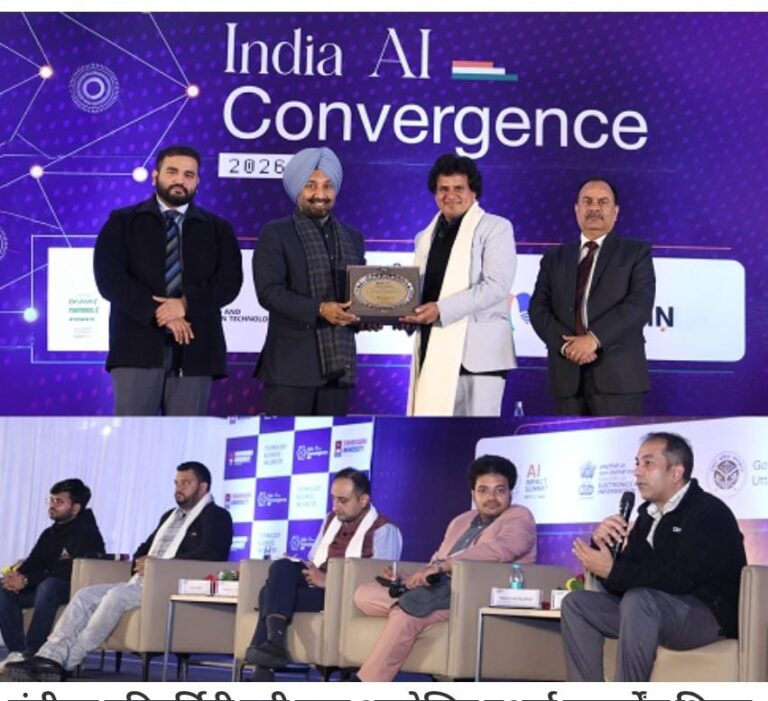(दिव्यराष्ट्र के लिए डॉ. पूजा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी)
आज का युग वैश्विक शिक्षा, ज्ञान-साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का युग है। जब विश्व की सीमाएँ तकनीकी और डिजिटल माध्यमों से सिकुड़ती जा रही हैं, तब शिक्षा का स्वरूप भी अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ओर अग्रसर है। इसी संदर्भ में “विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आगमन” एक नए दौर की शुरुआत है, जो न केवल भारत के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलेगा, बल्कि वैश्विक ज्ञान-आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित करेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने उच्च शिक्षा में स्वावलंबन और स्वदेशी संस्थागत निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम और बाद में अनेक राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना ने भारतीय शिक्षा को मजबूत किया। परंतु वैश्वीकरण के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से ही यह मांग उठने लगी कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को प्रवेश दिया जाए ताकि भारतीय छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा अपने देश में ही उपलब्ध हो सके।
नई शिक्षा नीति (नैप 2020) और अंतर्राष्ट्रीयकरण
2020 में घोषित नई शिक्षा नीति (नैप) भारत के शिक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है “शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण”। नेप 2020 ने पहली बार स्पष्ट रूप से यह अनुमति दी कि विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। नीति के अनुसार, यह कदम भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार क्षमता और शोध संस्कृति को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का यह प्रयास दोहरे उद्देश्य से प्रेरित है-पहला, भारतीय छात्रों को विदेशी शिक्षा के समान अवसर अपने ही देश में उपलब्ध कराना ताकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली वैश्विक शिक्षा के लिए विदेश न जाना पड़े; और दूसरा, भारत के शिक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खोलना, जिससे देश में शैक्षणिक नवाचार, शोध और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिल सके। इस नीति के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने भौतिक कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है, साथ ही उन्हें कुछ प्रशासनिक और नियामक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है ताकि वे अपने वैश्विक मानकों, शिक्षण पद्धतियों और शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रख सकें।
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन की प्रक्रिया
2023-24 के दौरान भारत सरकार और यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश सुनिश्चित करते हैं कि केवल प्रतिष्ठित, उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान-जैसे ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, या सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ही भारत में प्रवेश कर सकें। इन संस्थानों को अनुमति प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि वे विश्व के शीर्ष संस्थानों में से हैं, उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है, और वे भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा करेंगे। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है।
पाठ्यक्रम, शोध और शिक्षण पद्धति को उन्नत करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे देश में “अकादमिक उत्कृष्टता” का एक नया मानक स्थापित होगा। साथ ही, यह कदम प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को रोकने में सहायक होगा क्योंकि अब छात्र विश्वस्तरीय शिक्षा अपने देश में ही प्राप्त कर सकेंगे, जिससे ब्रेन गेन को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से वैश्विक नेटवर्किंग और अनुसंधान सहयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारतीय शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा और आर एंड डी संस्कृति को नई दिशा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों के कारण रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे तथा आधुनिक, स्किल-आधारित शिक्षा से छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। अंततः, शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत ग्लोबल एजुकेशन हब” बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा।
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से जहाँ अनेक अवसर उत्पन्न होंगे, वहीं कई संभावित चुनौतियाँ भी सामने आएँगी। सबसे पहले, नियामक और नीति-संबंधी बाधाएँ एक बड़ी चुनौती हैं क्योंकि विदेशी संस्थानों को भारत की जटिल प्रशासनिक और नौकरशाही प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जो अक्सर धीमी और अस्पष्ट होती हैं। दूसरी ओर, सामाजिक और आर्थिक असमानता का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालयों की फीस सामान्य भारतीय संस्थानों की तुलना में अधिक होगी, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए इन तक पहुँच कठिन हो जाएगी और शिक्षा में “वर्गीय असमानता” गहराने की आशंका रहेगी। तीसरी चुनौती सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान से जुड़ी है; विदेशी शिक्षा मॉडल भारत की विविध सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पृष्ठभूमि से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा और स्वदेशी दृष्टिकोण को हाशिये पर जाने का खतरा है। अंततः, विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति से स्थानीय निजी विश्वविद्यालयों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ेगा, और यदि वे गुणवत्ता सुधार में असफल रहे तो उन्हें छात्र संख्या में कमी और वित्तीय संकट जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
यह स्थिति भारतीय संस्थानों के लिए “खतरा” नहीं बल्कि “अवसर” भी हो सकती है। विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति उन्हें आत्ममंथन और नवाचार के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय विश्वविद्यालय अब अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, द्विगुणीय डिग्री प्रोग्राम, और अनुसंधान विनिमय जैसी पहलों में शामिल होकर अपनी वैश्विक पहचान बना सकते हैं। आईआईटी मद्रास ने ज़ांज़ीबार में अपना पहला विदेशी कैंपस खोला है। अमृता विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और अशोका विश्वविद्यालय पहले से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में सक्रिय हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। उनके पाठ्यक्रमों को भारतीय शिक्षा की विविधता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग और यूजीसी को एक संतुलित नियामक ढाँचा बनाना चाहिए जिससे गुणवत्ता नियंत्रण तो हो, पर अत्यधिक नियंत्रण से नवाचार बाधित न हो। इसके अलावा, छात्रवृत्ति योजनाएँ , क्रॉस-क्रेडिट सिस्टम, और वैश्विक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों के साथ तालमेल भी ज़रूरी होगा। यह सब मिलकर “ग्लोबल एजुकेशन इकॉनमी” में भारत को नेतृत्व की स्थिति दिला सकता है।
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन केवल शिक्षा की घटना नहीं है- यह वैचारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत है। यह परिवर्तन भारत को “ज्ञान-आधारित समाज की दिशा में आगे ले जाएगा। हालाँकि चुनौतियाँ मौजूद हैं-जैसे समानता, सांस्कृतिक संतुलन और प्रशासनिक स्पष्टता, परंतु यदि नीति निर्माण और क्रियान्वयन दूरदृष्टि से किया गया, तो भारत निकट भविष्य में “ग्लोबल एजुकेशन डेस्टीनेशन बन सकता है। जैसे-जैसे भारत अपनी युवा शक्ति, तकनीकी नवाचार और नीति सुधार के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का यह नया दौर भारतीय शिक्षा को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने की क्षमता रखता है।